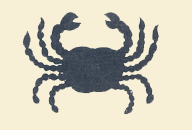हेपेटाइटिस बी आज एक स्वास्थ्य समस्या के रूप मे उभर कर सामने आ रहा है। हेपेटाइटिस बी से फैलने वाला पीलिया का रोग शुरू से समय तो अन्य हेपेटाइटिस वायरस के समान ही होते है। जैसे रोगी व्यक्ति का शरीर दर्द करता है, हल्का बुखार, भूख कम हो जाती है। उल्टी होने लगती है। इसके साथ ही पेशाब का व आंखो का रंग पीला होने लगता है।
प्र. हेपेटाइटिस (पीलिया ) के लक्षण क्या है ?
उ.-
-हल्का बुखार, बदन दर्द
- भूख कम लगना
- उबकाई व उल्टी
- पीली ऑखे व पीला पेशाब
प्र. राजस्थान मे हाडोती मे इन दिनों दो स्थानों पर अचानक पीलिया के अधिक रोगी एक साथ हो गये उसका क्या कारण है?
उ. अचानक जब कभी एक स्थान पर पीलिया के रोगी अधिक हो जाते हे उसे पीलिया का एपिडेमिक कहा जाता है। इन दोनो स्थानों पर गंदे नाले के टूटने से दूषित जल के स्वच्छ पीने के पानी मे मिल जाने से पीलिया वायरस ई के कीटाणु फैल गये।
प्र. क्या हेपेटाइटिस ए वयस्को मे भी हो जाता है?
उत्तर . जी हॉ, यह वयस्को में हो सकता है। ऐसा पाया गया कि हेपेटाइटिस ए के वायरस रोगी व्यक्ति के मल से विसर्जित होकर धूल-मिट्टी में मिल जाते है। जब बच्चे खेलते -कूदते उनके सम्पर्क में आते हैं तो स्वस्थ बच्चे में हल्की मात्रा में वायरस पहुंच कर उसके खिलाफ प्रतिरोधात्मक शक्ति बना देते है, मगर जब से सभ्रान्त, धनी परिवार के बच्चे ऐसी धूल-मिट्टी के सम्पर्क में नही आ पाते है तो यह प्रतिरोधात्मक शक्ति नही बन पाती वयस्क उम्र में ऐसे बच्चों को हेपेटाइटिस ए होने की संभावना बढ जाती है।
प्र. यह हेपेटाइटिस बी का वायरस किस प्रकार फैलता है?
उ. साधारणतया यह वायरस रोगी के रक्त मे रहता है जब भी स्वस्थ व्यक्ति रोगी के दूषित रक्त से संक्रमित इंजेक्शन की सुई बिना टैस्ट किये खून चढाने वास्ते उपयोग मे लेगा अथवा दूषित रक्त अगर पलंग पर जमा हो व किसी व्यक्ति की चमडी मे दरार होता उसमे प्रवेश कर जाता है।
सक्रमित मॉं के रक्त से नवजात शिशु के सम्पर्क मे आने से बच्चें के भी सक्रमित हो जाने की सभावना होती है।
सक्रंमित खून, इजेंक्शन सुई चढाने से मॉ से बच्चे में।
प्र. आपने संक्रमण या रोग फैलने के कारण बताये क्या ऐसी सावधानियां है जिन्हे आम आदमी को व्यवहार मे बरतना चाहिए?
उ.सभी व्यक्तियो को निम्न सावधानियां रखनी चाहिए -
- किसी चोट लगे व्यक्ति से खून के सम्पर्क मे आने पर या संक्रमित सुई चूभ जाने पर या रक्त के हाथ पर गिर जाने पर।
- सभी पैरामैडिकल व डाक्टर्स मरीजों के घावो के इलाज के समय या ऑपरेशन के समय या रक्त सम्बन्धित टैस्ट करते समय।
- सदैव सुरक्षित, कीटाणु रहित नई व सिरिज का उपयोग करे ग्लास सिरिंज व सुई 15 -20 मि. तक उबाल कर उपयोग करे।
-सदैव रक्त चढाने से पूर्व जॉचे कि रक्त हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रति जांचा हुआ है।
- सुरक्षित यौन सम्बन्ध रखे पर स्त्री गमन न रखे या बार-बार साथी न बदले या ऐसे समय कन्डोम का उपयोग रखें।
प्र. इनके अलावा क्या कोई और उपाय है, जिससे बचाव हो सकता है?
उ. सावधानियों के अलावा रोग से प्रतिरोध करने वाले एण्टीबाडीज भी वैक्सवीनेशन द्वारा पैदा किये जा सकते है।
- ऐसे सभी व्यक्ति जिनमे हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूदा नही है सभी उम्र व लिंग के व्यक्तियो को टीके लगवाना चाहिए।
-सभी नवजात शिशु को।
- हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित मां से उत्पन्न संतान को।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस टीके को ई.पी.आई. प्रोग्राम में शामिल किया है।
-टीका डेल्टाईट मॉंसपेशी (बायें हाथ की ऊपरी भुजा भाग में ही लगाना चाहिए)।
-यह 1 उस मात्रा में 17 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में व
-0.5 उस मात्रा 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में।
प्रथम टीका एक निश्चित तारीख।
द्वितीय टीका प्रथम टीके के एक माह बाद।
तृतीय टीका प्रथम टीके के 6 माह बाद लगवायें एक बार टीका लगाने के बाद एण्टीबॉडीज लगभग 10 वर्ष तक बनी रहती है।
दुबारा टीका लगाने की आवश्यकता नहीं होती।
हेपेटाइटिस बी से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी आप हमारे पाठकों को देना चाहिए।
-भारत में इससे 3 से 5 प्रतिशत व्यक्ति एच.आई.वी. से संक्रमित हैं।
-हर 20 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति इससे ही ग्रसित है।
-लगभग 3 से 4 करोड व्यक्ति एच.आई.वी. से प्रभावित है।
-संक्रमित रोगियों में से आधों को यकृत सिरहासिस व यकृत कैंसर हो सकता है।
- तम्बाकू से द्वितीय कारण कैंसर या हैपेटाईटिस बी का संक्रमण है।
टीके लगवा कर इससे बचा जा सकता है।
-यह रोग भी एडस के समान अनियंत्रित यौन संबंधों से फैलता है।
-यह एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि:-
- जहां एड्स के लिये 0.1 मि.ली. संक्रमित रक्त चाहिए वहां केवल 0.0001 मि.ली. यानि सूक्ष्म माञा से रोग फैल सकता है।
-यह एड्स वायरस से 100 गुना अधिक संक्रमित करने की क्षमता रखता है।
- जितने रोगी एड्स से एक साल में मरते हैं उतने हेपेटाइटिस बी में एक दिनमें मर जाते हैं।
हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाकर बचा जा सकता है, एड्स का बचावी टीका उपलब्ध नही है।
प्र0 अपने बच्चे को हेपेटाइटिस बी से कैसे बचाये?
उ0 पीलिया जॉन्डिस का रोग सदियो से चला आ रहा है परन्तु केवल इस सदी मे ही पीलिया के विभिन्न कारणों का वर्णन हुआ है और इसका श्रेय जाता है मेडिकल तेकनालाजी मे हूई महत्वपूर्ण प्रगति को।
मेडिकल जान्डिस का आम कारण है वाइरल हेपेटाइटिस इस नाम के दो पहलू है वाइरल, यानी इस रोग का कारण वाइरस है और हेपेटाइटिस, जिसका अर्थ है कि यकृत (लीवर) मे सूजन है।
आमतौर पर लोगो की धारणा है कि सभी यकृत की बीमारिया शराब की अधिक माञा मे लेने से होती है। दरअसल 80 प्रतिशत हेपेटाइटिस का कारण है वाइरल संक्रमण अक्सर हेपेटाइटिस एक लक्षणहीन रोग होता है जिसके कोई बाहरी चिन्ह नजर नही आते हैं परन्तु हेपेटाइटिस का इलाज न हो तो रोगी लीवर फेलियर से कोमा मे पहुंच सकता है ओर अन्त मे उसकी मृत्यु हो सकती है।
 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
Department of Medical, Health & Family Welfare
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
Department of Medical, Health & Family Welfare


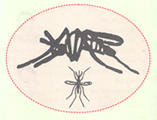
 रोग का प्रसार कैसे?
रोग का प्रसार कैसे?